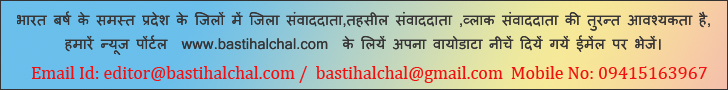डॉ. वेदप्रताप वैदिक —
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने डाॅ. कफील खान को रिहा करने का फैसला दिया था, उस पर मैंने जो लेख लिखा था, उस पर सैकड़ों पाठकों की सहमति आई लेकिन एक-दो पाठकों ने काफी अमर्यादित प्रतिक्रिया भी भेजी। उन्होंने इसे हिंदू-मुसलमान के चश्मे से देखा। मेरा निवेदन यह है कि न्याय तो न्याय होता है। वह सबके लिए समान होना चाहिए। उसके सामने मजहब, जात, ओहदा और हैसियत आदि का कोई ख्याल नहीं होना चाहिए। यदि डाॅ. कफील खान की जगह कोई डाॅ. रामचंद्र या डाॅ. पीटर होते तो भी मैं यही कहता कि वे दोषी हों तो उन्हें दंडित किया जाए और निर्दोष हों तो उन्हें सजा क्यों दी जाए ? यह कानून दिसंबर 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार ने बनाया था। इसका असली मकसद क्या रहा होगा, यह कहने की जरुरत नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के नाम पर आप किसी को भी पकड़कर जेल में डाल दें, यह उचित नहीं। गिरफ्तार व्यक्ति को साल भर तक न जमानत मिले, न ही अदालत उसके बारे में शीघ्र फैसला करे, यह अपने आप में अन्याय है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून आखिर किसलिए लाया गया था? दावा किया गया था कि इससे भारतीय संविधान की व्यवस्था सुरक्षित रहेगी। देश में कोई बड़ी अराजकता न फैले, किसी विदेशी शक्ति के साथ सांठ-गांठ करके कोई देशद्रोही गतिविधि नहीं चलाई जा रही हो या देश की शांति और व्यवस्था को भंग करने की कोशिश न की जाए। जिन प्रादेशिक और केंद्र सरकार ने इस कानून के तहत सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है, क्या देश में इतने देशद्रोही पैदा हो गए हैं? इन तथाकथित देशद्रोहियों में हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। किसी को कोई भाषण देने पर, किसी को लेख लिखने पर और किसी को किसी प्रदर्शन में भाग लेने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। एक व्यक्ति को सांप्रदायिक तनाव फैलाने की आशंका में पकड़ लिया गया, क्योंकि उसके खेत में किसी पशु का कंकाल मिल गया था। इस तरह की गिरफ्तारियां इस कानून का पूर्ण दुरुपयोग है। वास्तव में इस कानून का इस्तेमाल बहुत गंभीर अपराधियों के विरुद्ध होना चाहिए लेकिन सत्तारुढ़ लोग अपने विरोधियों के विरुद्ध इसे इस्तेमाल करने में जरा भी नहीं चूकते। 1977 में अपदस्थ होने के बाद इंदिराजी यह कानून इसी डर के मारे लाई थीं कि कहीं वही इतिहास दुबारा नहीं दोहराया जाए। यह कानून अंग्रेजों के ‘रोलेट एक्ट’ की तरह दमनकारी है। इसे ‘डीआईआर’ और ‘मीसा’ की श्रेणी में रखा जा सकता है। यह ‘रासुका’ संविधान की मूल भावना से मेल नहीं खाता। इसका क्रियान्वयन इतना गड़बड़ है कि संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का यह अक्सर उल्लंघन कर देता है। सरकार इस पर पुनर्विचार कर सकती है। यह आपात्काल की अवांछित संतान है।
(लेखक ‘डीआईआर’ के तहत 1965 में छात्र—नेता की तरह जेल काट चुके हैं)